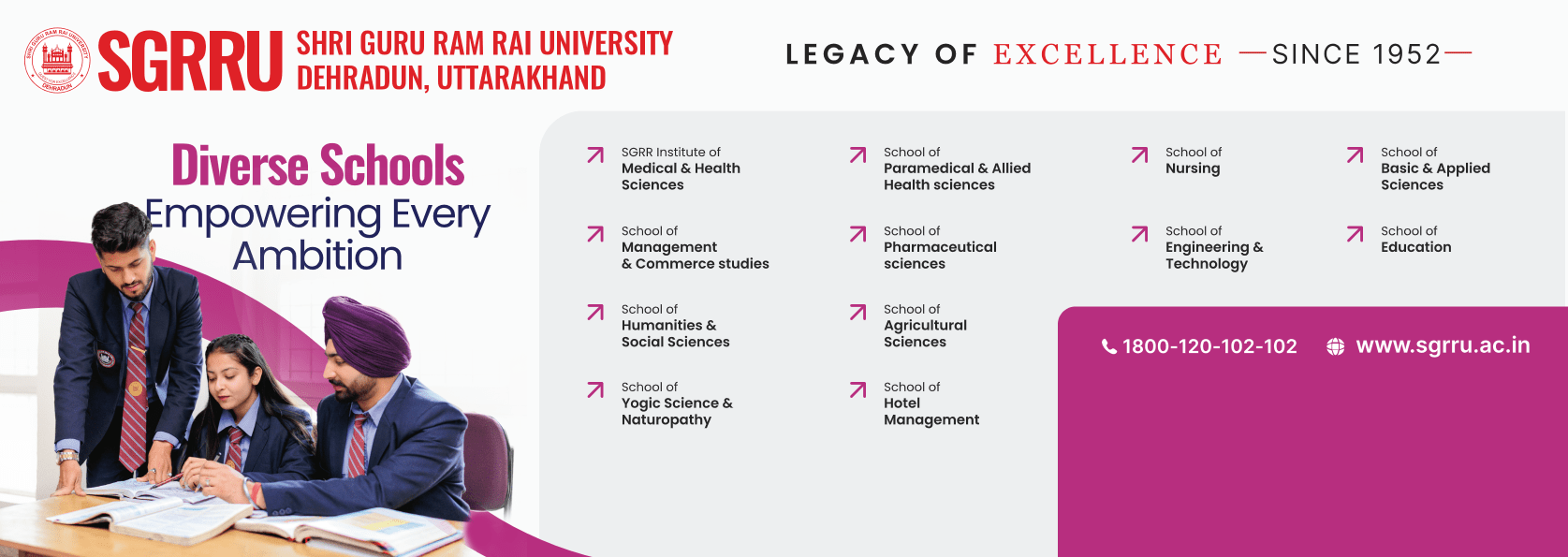स्मृति शेष-स्व.शिबू सोरेन
झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पाल की कलम से
1855 में जब सिदो-कान्हू, चांद-भैरव, और फुलो-झानो ने ‘दामिन-ए-कोह’ की धरती पर अंग्रेज़ी राज, महाजनों और जमींदारों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका, तो वह सिर्फ हथियारबंद विद्रोह नहीं था, वह एक नई शासन व्यवस्था की माँग थी—जिसमें आदिवासी समाज अपने तरीके से जी सके, अपने नियम बना सके और अपनी ज़मीन, जंगल और संस्कृति की रक्षा कर सके।
इसी विचार की एक और कड़ी शिबू सोरेन की चेतना में दिखाई देती थी। शिबू सोरेन का प्रारंभिक संघर्ष भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा संथाल विद्रोह का — महाजनों के खिलाफ, ज़मींदारों के शोषण के खिलाफ, और पुलिसिया अत्याचारों के विरुद्ध।
उन्होंने ‘धान काटो आंदोलन’, जंगल में समाज सुधार सभाएं, शराबबंदी अभियान, बाल विवाह विरोधी आंदोलन जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए। शुरुआत में उनका आंदोलन उग्र था — हिंसा भी हुई, पुलिस से टकराव हुआ। लेकिन फिर के.बी. सक्सेना जैसे अधिकारियों के हस्तक्षेप और शिबू सोरेन की वैचारिक परिपक्वता के कारण यह आंदोलन लोकतांत्रिक दिशा में मुड़ा।
जहाँ संथाल विद्रोह में राजा की जगह आदिवासी ग्राम प्रमुख की कल्पना थी, वहीं शिबू सोरेन के आंदोलन में भी गांवों की संप्रभुता की मांग थी। जहाँ संथाल विद्रोह में हूल’ था, वहाँ शिबू सोरेन के आंदोलन में हुंकार थी—लेकिन उद्देश्य एक था-हम अपनी ज़मीन, जंगल और आत्मा पर किसी बाहरी सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे।
शिबू सोरेन सिर्फ एक नेता नहीं हैं, वे उस क्रांति का नाम हैं, जो ज़मीन की गंध से उठी थी और संसद तक पहुंची। जब भारत की राजनीति में हाशिए पर खड़े समुदायों की बात होती है, तो झारखंड के आदिवासियों की पीड़ा और प्रतिरोध की गाथा में एक नाम सबसे पहले उभरता है—शिबू सोरेन।
वे सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि झारखंड के जनांदोलन के प्रतीक हैं। उनका जीवन, उनके विचार और उनके संघर्ष आदिवासी अस्मिता, जमीन, जंगल और जल की रक्षा के लिए खड़े हुए उस विराट आंदोलन का हिस्सा है, जिसने एक राज्य को जन्म दिया और हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज़ दी।
एक विचारधारा की लंबी यात्रा
संथाल विद्रोह और शिबू सोरेन का आंदोलन एक ही श्रृंखला की दो कड़ियाँ हैं। एक चेतना जो “हम अपने मालिक खुद हैं” के विश्वास से जन्मी थी। फर्क केवल समय, भाषा, राजनीति और रणनीति का है। 1855 में वह चेतना हूल थी, 1970 में हक़ बन गई, और आज वह संवैधानिक अधिकारों की मांग के रूप में खड़ी है। पर सवाल वही है—
• क्या झारखंड के आदिवासी अब भी मालिक हैं?
• क्या उनकी ग्राम सभाएं अब भी निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं?
• क्या खनिज सम्पदा से उन्हें कोई लाभ मिल रहा है?
अगर इन सवालों के जवाब ‘ना’ हैं, तो हमें फिर से हूल की आत्मा और गुरुजी की रणनीति को याद करना होगा।