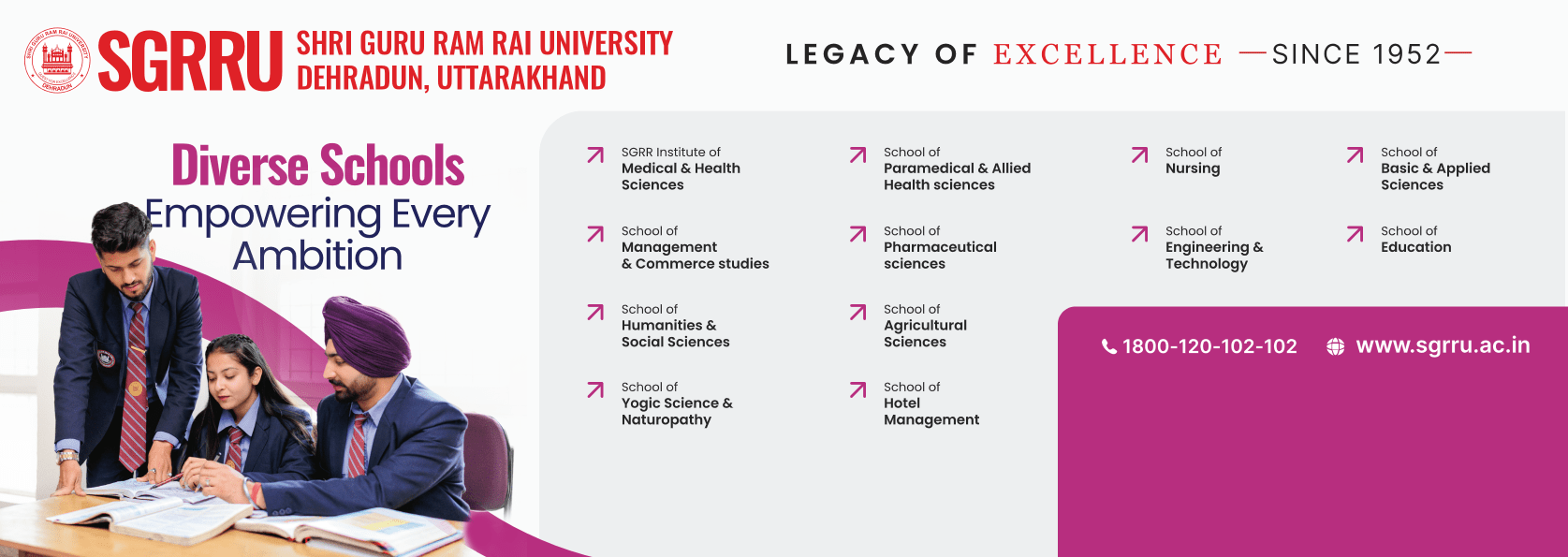दिनेश शास्त्री
देहरादून। उत्तराखंड इन दिनों रजत जयंती उत्सवों की थकान उतार रहा है। जवानी के 25 वर्ष हिलोरें लेने के होते हैं।
गोपाल बाबू गोस्वामी ने वर्षात के दिनों में लबालब नैनी झील को प्रतीक बना कर गीत रचा था – “जवानी म भर्यु रे छो जसो नैनीताल”। यानी भरपूर जवानी, पहाड़ पर फतह कर लेने का जज्बा।
इन 25 सालों में विकास खूब हुआ, ये दावे के साथ कहा जा सकता है लेकिन किसका हुआ? ये सवाल न पूछें तो अच्छा है। पहाड़ आज भी विकास की आस लगाए हुए हैं। प्रमाण देखने के लिए ज्यादा दूर क्यों जाना? बागेश्वर जिला मुख्यालय से मात्र 23 किमी दूर बसे चौनी गांव के आखिरी परिवार ने इसी रजत जयंती वर्ष में नम आंखों से अपनी माटी को अलविदा कहा।
पलायन पर चर्चा बहुत होती रही है।
दरअसल पलायन के कारण ही इस हिमालयी प्रदेश के लिए आंदोलन हुआ था लेकिन ये पता न था कि अलग राज्य बनने के बाद गांव सूने होने लगेंगे। पिछले 25 वर्षों में खाली होने वाले गांवों में चौनी का नंबर 1793 वां है। इससे पहले 1792 गांव निर्जन हो चुके हैं।
यह अलग उत्तराखंड राज्य बनने के बाद की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। गांव ऐसी स्थिति है जिसे अत्यंत मजबूरी में ही छोड़ा जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और जीविका मुख्य पैमाने हैं।
उत्तराखंड में पलायन की समस्या पहले से रही है लेकिन ये स्थिति कभी नहीं आई थी कि गांव के गांव खाली हो जाएं। जब घोर निराशा की स्थिति आती है, तब गांव छोड़ा जाता है। वह अंतिम विकल्प होता है।
राज्य सरकार ने पलायन की समस्या जानने के लिए 2018 में पलायन आयोग गठित किया था। उसका मुख्यालय पौड़ी बनाया गया लेकिन आयोग को खुद पलायन कर देहरादून ठिकाना बनाना पड़ा। वर्ष 2018 से 2022 तक की अवधि में 24 नए गांव निर्जन हुए। पौड़ी और अल्मोड़ा तो पहले ही घोस्ट विलेज के लिए बदनाम थे। टिहरी का चम्बा ब्लॉक उसमें और दर्ज हो गया और इस तरह चौनी गांव ने आखिरकार 1793वां स्थान दर्ज कर लिया।
कहने को गांवों में मानव आदिवास स्थिर रखने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई किंतु उन योजनाओं में इतने छेद रहे कि भरने मुश्किल हो गए। मुख्य कारण पहाड़ में खेती करना दुष्कर हो गया है। वन्य जीवों के हमले, खेती को नुकसान और उत्पादन लागत के मुताबिक दाम न मिलना नकारात्मक बिंदु हैं। वन्यजीवों के हमले में कोई व्यक्ति घायल हो जाए तो सरकार के खर्च पर उसके इलाज की व्यवस्था का दावा तो है लेकिन वन्य जीव आबादी क्षेत्र में दहशत का सबब न बने, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
पहाड़ों में उत्पात मचा रहे बंदरों के बारे में एक आम धारणा बन गई है कि जब जब हरिद्वार में कुम्भ पर्व होता है तो उन बंदरों को पहाड़ में भेज दिया जाता है। ये बात कितनी सत्य है, यह तो वन विभाग ही बता सकता है किंतु पहाड़ में अब पाए जा रहे बंदरों का हिंसक व्यवहार कम से कम इस आशंका की एक तरह से पुष्टि ही करता है। पौड़ी जिला गुलदार के आतंक से त्रस्त है तो चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी आजकल भालुओं के खौफ के साए में हैं। उत्तरकाशी में 11 लोगों को भालू लहूलुहान कर चुके हैं जबकि दो लोगों की जान ले चुके हैं। चमोली में आधा दर्जन घटनाएं इसी तरह की हो चुकी हैं। सरकारी फरमान है कि आबादी क्षेत्रों से झाड़ियां हटाई जाएं, किंतु लाख टके का सवाल है कि क्या इतने भर से भालू का आतंक खत्म हो जाएगा?
रिवर्स माइग्रेशन के नाम पर सरकार ने जो कोशिशें की, वह एक भी सिरे नहीं चढ़ी। कोविड़ के दौरान पौने तीन लाख पहाड़ी घर लौटे थे। ये आंकड़ा तब की त्रिवेंद्र सरकार ने जारी किया था। स्थिति सामान्य होने के बाद किसी का भी ठहराव पहाड़ में करने में सरकार विफल रही। पलायन आयोग ने खुद माना है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में वित्तीय सीमाएं,भ्रष्टाचार और विभागीय समन्वय की कमी जैसी बाधाएं बरकरार हैं, किंतु उन्हें दूर करने के प्रति गंभीरता किसी भी स्तर पर नजर नहीं आती।
इस हालत में इंतजार कीजिए पहाड़ की डेमोग्राफी चेंज का। अगले परिसीमन में इस हालत में पहाड़ की दस सीटें और कम हुई तो दस नेता तो कम हो ही जाएंगे। जनता का क्या, वह तो पलायन के लिए अभिशप्त है। नेताओं को अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। इलाज एक ही है कि एक खूबसूरत शहर देहरादून को नरक बनाने के बजाय राजधानी गैरसैंण ले जाने की हिम्मत दिखाइए तो पहाड़ भी बचेंगे, पलायन भी रुकेगा और देहरादून भी। हालांकि होना वही है, जो नौकरशाही चाहेगी क्योंकि नौकरशाही अब इस मिजाज की नहीं है कि वह गैरसैंण के प्रारंभिक कष्ट सहन कर सके। लिहाजा भाग्य को कोसने के अलावा कुछ शेष नहीं है।